ताज़ा उदाहरण चुनाव आयोग का है । जिसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल पिछले कुछ सालों से उठ रहे हैं । आयोग के बारें में ये कहा जाने लगा कि वो सरकार की मुठ्टी में है । उनके इशारे पर ही फ़ैसले आते हैं और जो भी चुनाव आयुक्त सरकार या सत्ताधारी पार्टी की बात से इत्तफ़ाक़ नहीं रखता या फिर उनका पक्ष नहीं लेता तो फिर उसे सजा के लिये तैयार रहना चाहिये ।
अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहिये था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के एक मामले में वो प्रधानमंत्री के कथन से सहमत नहीं हुए और आयोग के बहुमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने की हिमाक़त की तो फिर उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाँच एजेंसियाँ पहुंच गई और आख़िर में उन्हें समय से पहले ही आयोग को छोड़ना पड़ा ।
आयोग की नियुक्ति अभी तक सरकार करती थी । इसके बावजूद उसका रुतबा काफ़ी था । लेकिन मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें अपने दफ़्तर बुलाने की ग़ुस्ताख़ी की जैसे कि वो सरकार के अधीनस्थ कोई विभाग हो । मीडिया में खबर आने के बाद आधी अधूरी सफ़ाई दी गई । और वो मीटिंग नहीं हुई । कई चुनावों की तारीख़ों की घोषणा में प्रधानमंत्री की रैलियों के ख़त्म होने तक इंतज़ार करने के आरोप लगे और उसमें काफ़ी सचाई भी दिखी । ऐसे में जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलिजियम बनाने की बात की तो फिर उम्मीद जगी कि अब आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को सरकार के दायरे से निकाल कर नई व्यवस्था दी ताकि आयोग की चयन प्रक्रिया को कठघरे में न खड़ा किया जा सके । कोर्ट ने कहा कि आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों की एक कमेटी करेगी । जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष होंगे । अदालत ने ये भी कहा कि सरकार को इस बारे में क़ानून बनाना चाहिये । अब सरकार क़ानून का जो मसौदा लेकर आई है उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया है । ज़ाहिर हैं व्यवस्था फिर वहीं हो गई जिससे सुप्रीम कोर्ट निकलना चाहता था । यानी चुनाव आयोग में आयुक्त सरकार की मर्ज़ी से ही नियुक्त होंगे । तो फिर कोर्ट के फ़ैसले का मतलब क्या रहा गया ? सरकार ने कोई सफ़ाई नहीं दी है, और न वो देना चाहती है कि उसे मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी पर क्या आपत्ति थी ? क्या सरकार को मुख्य न्यायाधीश पर ही भरोसा नहीं है कि वो निष्पक्ष आयुक्त बनाने में सही भूमिका निभायेंगे ?
दरअसल, ये एक मानसिकता है । जिसकी वजह से देश में संविधान द्वारा बनायी गई संस्थाएं मज़बूत न हो, ये कोशिश लगातार होती रहती है । ये कोशिश हर सरकार और हर प्रधानमंत्री करता है । उनको ये गुमान होता है कि देश चलाने की अकेले ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनकी है, बाक़ी की नहीं । जब कि ‘राज्य’ सिर्फ़ सरकार का नाम नहीं होता, वो न्यायपालिका भी है और विधायिका भी, वो रिज़र्व बैंक भी है और चुनाव आयोग भी, वो पुलिस भी है और आयकर विभाग भी, वो लोकपाल भी है और मानवाधिकार आयोग भी और न जाने और कितनी संस्थाओं का वो समुच्चय है । लेकिन अगर सरकार का मुखिया सोचने लगे या मान बैठे कि उनके अलावा बाक़ी सारी संस्थाओं को उनके इशारों पर डांस करना चाहिये, और वो वही करें जो उनको कहा जाये तो फिर संस्थाओं का पतन निश्चित है । जब ये सोच हावी हो जाती है कि संस्थाओं के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे जो सरकार की कठपुतलियाँ हों, रोबोट हों, जो अपने फ़ैसले न ले, वो सिर्फ़ सरकार के कहे पर चलें, तो फिर देश एक नये संकट की और बढ़ने लगता है ।
ये प्रवृत्ति अपने स्वभाव में लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है और देश विरोधी भी । ये अपने ही देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश है । क्योंकि इस कारण देश की तमाम संस्थाओं को न तो पनपने दिया जाता है और न ही उनके शीर्ष पदों पर क़ाबिल लोगों की नियुक्ति होती है। ग़ुलाम बनने को वही तैयार होते हैं जिनकी अपनी अक़्ल और चरित्र, दोनों ही गिरवी होते हैं ।
ये व्यवस्था मिडियाक्रिटी को बढ़ावा देती है और जो समाज अपने मेधावी और जीनियस लोगों की मेधा का इस्तेमाल नहीं करती वो धीरे धीरे पिछड़ती जाती है । नेहरू ने जब देश की कमान सँभाली थी तब देश कंगाल था, वो भुखमरी, ग़रीबी, निरक्षरता से जूझ रहा था, और तब कई विदेशी विद्वान ये कामना कर रहे थे कि देश कुछ सालों में टूट जायेगा । लेकिन नेहरू ने लोकतंत्र की जो नींव रखी, ये उसका परिणाम है कि आज भी देश में समय पर चुनाव होते हैं और जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इतिहास ने उनको माफ़ नहीं किया । और आज भी वो मोदी और बीजेपी की आलोचनाओं का शिकार होती रहती हैं ।
“इंदिरा की आलोचना हर प्रधानमंत्री को एक चेतावनी है कि देश तानाशाह को पसंद नहीं करता और जो भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश या साजिश करेगा या करेगी, उसका नाम इतिहास में खलनायक के तौर पर ही दर्ज होगा, वर्तमान में भले ही चमचे और दरबारी उनको महामानव बनाने की कोशिश करे ।
बाबा साहेब आंबेडकर ने यू ही नहीं कहा था कि ‘लोकतंत्र सिर्फ़ सरकार नहीं है, ये बुनियादी तौर पर साझी ज़िंदगी जीने की प्रक्रिया है, साझा संप्रेषणीय अनुभव है ।’ जो सरकार सबको साथ लेकर चलती हैं, संस्थाओं पर क़ब्ज़े की नहीं बल्कि सहकार की भावना से आगे बढ़ती है, वो साझे अनुभव का तिरस्कार नहीं करती, वो साझी संवेदना का सम्मान करते हुए भारत देश को आगे बढ़ाती है । जो ऐसा नहीं करती वो शासन तो भले कर ले, पर देश को पीछे ही ले जाते है ।

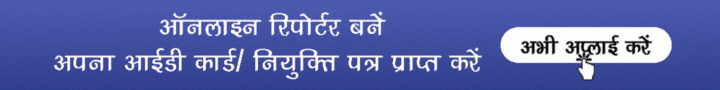


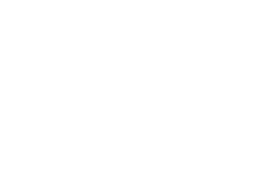 Subscribe Us
Subscribe Us

















